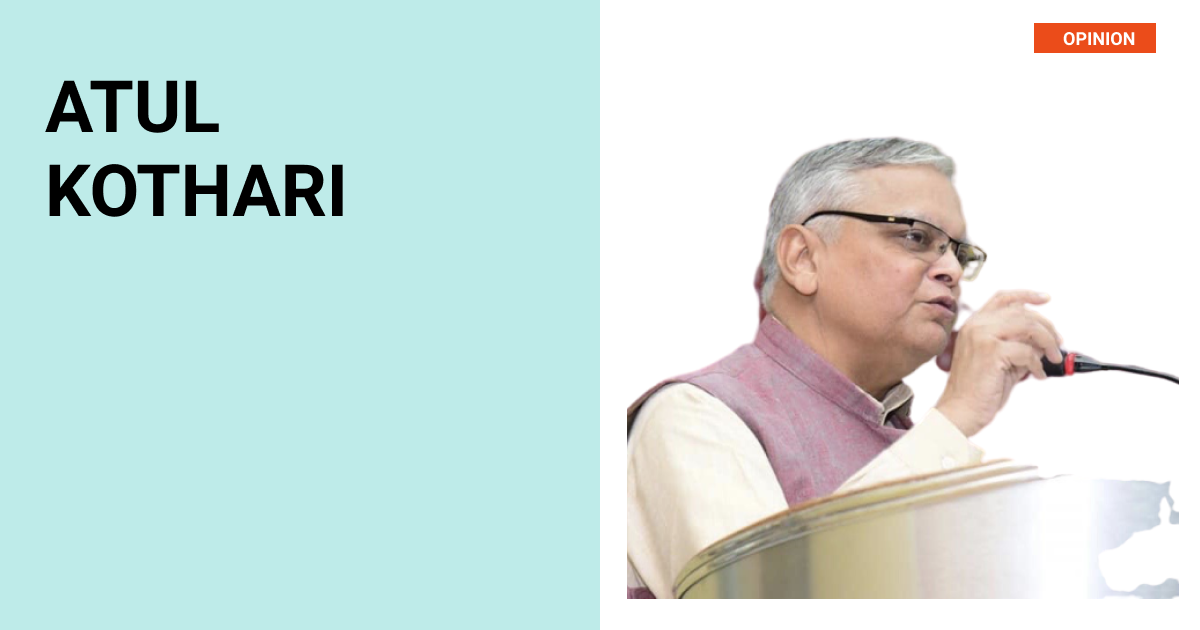समग्र विश्व को चीन से पनपे कोरोना नाम की एक नई चुनौती ने मानव समुदाय को संकट में डाल दिया है। एक तरफ़ मनुष्य स्वयं एवं उसके परिवार का जीवन संकट में है, दूसरी तरह से इस महामारी के कारण व्यक्ति से लेकर राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इसी प्रकार समग्र शिक्षा तंत्र ठप्प हो गया है। जिस प्रकार लोगों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अर्थ के बिना काम नहीं चल सकता, इसी प्रकार देश में अर्थ का अभाव एवं अति प्रभाव भी न हो अर्थात् धर्माधिष्ठीत अर्थव्यवस्था हो, यह कार्य बिना शिक्षा संभव नहीं है।
आज हमारी सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था संकट में है। कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं अधिकतर मात्रा में सम्पन्न हुई है परन्तु पूर्ण नहीं हो पायी है। इसके अतिरिक्त अन्य परीक्षाएं नहीं हो पाई है, कुछ राज्यों ने बोर्ड और अन्तिम वर्ष की परीक्षाओं को छोड़कर बाकी सारे छात्रों को बिना परीक्षा आगे के वर्ष में प्रवेश देने (मास प्रमोशन) की बात कही है। कुछ राज्यों एवं विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन परीक्षा की योजना पर विचार किया है। वैसे ऑनलाइन परीक्षाएं मात्र परीक्षा की औपचारिकता ही होगी। इस महामारी के कारण विश्वविद्यालयों में चलने वाले शोध-अनुसंधान बंद है। छात्रों के व्यक्तित्व के समग्र विकास हेतु चलने वाली खेल, सांस्कृतिक एवं कला सम्बंधित गतिविधियां आदि भी ठप्प है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन, चिकित्सा क्षेत्र के विद्वानों का मत बन रहा है कि चीनी वायरस का यह संकट जल्दी समाप्त नहीं होने वाला है। कोरोना भी चलता रहेगा और हमारा काम भी साथ-साथ चलता रहेगा। इस महामारी के साथ तालमेल बैठाकर, आवश्यक सावधानियों का पालन करते हुए जीवन चलाने की आदत डालनी पड़ेगी। परन्तु समाज जीवन पुनः पूर्व जैसा सामान्य हो यह आसान नहीं है। समाज का बड़ा वर्ग भयभीत है।
इस हेतु पहला काम है कि समाज को भयमुक्त करना। दूसरी बात यह प्राकृतिक नियम है, जहां समस्या होती है वहीं समाधान है, जहां चुनौतियाँ होती है, वहां अवसरों की पूरी सम्भावनाएं होती हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि, ‘‘जीवन में आये अवसरों को व्यक्ति साहस एवं ज्ञान की कमी के कारण समझ नहीं पाता है।’’ इस हेतु हमने साहस एवं ज्ञान दोनों का परिचय देते हुए इस चुनौती को अवसर में बदलने हेतु कटिबद्ध होना होगा।
हमारे देश में शिक्षा क्षेत्र में लम्बे समय से ऑनलाइन शिक्षा की बात चर्चा में थी, कुछ छुट-पुट प्रयास भी हुए थे परन्तु इस महामारी के कारण आज बड़ी मात्रा में ऑनलाइन शिक्षा प्रारम्भ हो गई है। यू.जी.सी के अनुसार अगस्त के पूर्व कॉलेज प्रारम्भ नहीं होंगे। हमने यू.जी.सी को सुझाव दिया है कि जब भी शैक्षिक कार्य प्रारंभ होगा तब दो-दिन ऑनलाइन, दो दिन प्रत्यक्ष संस्थान में आकर पढ़ाई और एक दिन प्रोजेक्ट र्वक अर्थात् व्यवहारिक अनुभव हेतु शिक्षा, इससे हमारे यहां वर्षों से रटन्त प्रक्रिया से पढ़ाई का कार्य चलाया जा रहा है, उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। दो दिन ऑनलाइन में व्याख्यान होगा उसमें से निर्माण हुए प्रश्न एवं छात्रों को जो बातें समझ में नहीं आई उसके समाधान के साथ-साथ विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए दो दिन प्रत्यक्ष कक्षा होगी और चार दिन की पढ़ाई का व्यवहारिक अनुभव एक दिन के प्रोजेक्ट वर्क से होगा। इस प्रकार पढ़ाने की पद्धतियों (पेडागॉजी) में हम आधारभूत बदलाव कर सकते हैं।
सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को दो पारी में चलाना चाहिए जिससे सब मिलाकर हर दिन एक पारी में अधिक से अधिक 15 से 20 प्रतिशत छात्र ही प्रत्यक्ष संस्थान में आयेंगे। इससे शारीरिक दूरी की सावधानी सरल हो जाएगी, रास्तों में ट्रैफ़िक भी कम होगा। इतने वाहन कम चलने से प्रदूषण कम होगा आदि बहुत सारे लाभ हो सकते हैं।
ऑनलाइन शिक्षा की कुछ समस्याएं हैं, उसका समाधान बाकी रहे दो माह में हमने ढूंढना होगा। इस हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण करना आवश्यक होगा। सतत ऑनलाइन शिक्षा से छात्र तनाव में रहना, नींद न आना आदि स्वास्थ्य सम्बंधित समस्याओं के शिकार हो रहे है। इन समस्याओं के समाधान हेतु ऑनलाइन अध्ययन हेतु विद्यालय एवं उच्च शिक्षा के स्तर के विधि-निषेध के साथ पाठ्यक्रम तैयार करने होंगे। साथ ही पढ़ाने की पद्धतियों में भी बदलाव करना होगा। गांवों, जनजातीय क्षेत्रों में ऑनलाइन नेटवर्क कनेक्टीवीटी आदि समस्याएं होगी, गरीब छात्रों को मोबाइल डाटा खर्च की भी समस्या हो सकती है। इसके साथ ऑनलाइन शिक्षा मातृभाषा में दी जाए इन सब बातों की तैयारी करनी होगी।
पाठ्यक्रम
कोरोना के इस संकट में बड़ी मात्रा में विशेष रूप से छात्रा काफ़ी तनाव में है और स्वास्थ्य का संकट तो है ही इस हेतु स्वास्थ्य एवं योग शिक्षा को हर स्तर पर अनिवार्य करना होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के स्वावलम्बन एवं लोकल (स्थानीय) को वोकल करने की बात कही है, अर्थात् स्वदेशी का आग्रह। इस हेतु हमारे अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रमों में स्वदेशी एवं स्वावलम्बन सम्बंधित विषयों का समावेश करना होगा। आज अधिकतर कार्य ऑनलाइन चल रहे हैं, और आगे भी कम से कम एक वर्ष तो ऐसे ही चलना होगा। नासकोम के अध्ययन के अनुसार हमको 60 लाख से अधिक साइबर सिक्योरीटी के जानने वालों की आवश्यकता है। इस हेतु साइबर क्राइम के प्रति सावधान करने वाले पाठ्यक्रमों को भी अग्रीमता देनी होगी। इस प्रकार पाठ्यक्रम में बदलाव की तैयारी शीघ्रता से प्रारंभ करने की आवश्यकता है। जिससे अगस्त, सितम्बर तक पाठ्यपुस्तकें तैयार हो सकें।
कौशल शिक्षा (स्किल डेवेलप्मेंट)
वर्तमान पाठ्यक्रमों में व्यापक बदलाव आवश्यक है। प्रथम बात हर विषय के अनुसार कौशल शिक्षा के पाठ्यक्रम होने चाहिए। दूसरी बात राष्ट्रीय, सामाजिक एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार किए जाए। जिस प्रकार कुछ आई.आई.टी एवं अन्य शैक्षिक संस्थानों ने छोटे आकार के वेंटिलेटर, हैंड सैनिटाइजर, संक्रमितों की पहचान करने वाले ऐप एवं नर्स का कार्य करने वाले रोबोट, मास्क एवं आयुर्वेदिक काढ़े आदि वस्तुएं बनाकर दिए हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रमों का विचार करना होगा। साथ ही चिकित्सा सहायक, चिकित्सा उपकरण संचालक आदि जैसे पाठ्यक्रमों पर भी विचार किया जाना आवश्यक होगा।
स्वावलंबन एवं स्वदेशी
स्वावलम्बन एवं स्वदेशी का महत्वपूर्ण आधार कौशल शिक्षा (स्कील डेवेलप्मेंट), शोध् एवं अनुसंधान है। अमेरिका हो या विश्व के अन्य देश अधिकतर महत्वपूर्ण शोध विश्वविद्यालयों में ही होते हैं। आज अवसर है कि हम अपने विश्वविद्यालयों को इस प्रकार की दिशा प्रदान करें। इस हेतु शोध-अनुसंधान की प्रक्रिया में आधारभूत बदलाव करते हुए राष्ट्रीय, सामाजिक एवं स्थानीय आवश्यकता के अनुसार शोध हो साथ ही अपनी भाषाओं में शोध कार्य को प्राथमिकता देनी होगी।
ऑनलाइन शिक्षा हेतु आज भी हम विदेशी एप पर निर्भर है क्या भारत के आई.आई.टी जैसे संस्थानों के द्वारा भारतीय ऐप नहीं बनाये जा सकते? इस महामारी के इलाज हेतु जैसे हमने अमेरिका सहित अनेक देशों को हाइड्रोक्लोरोक्विन दवाएं उपलब्ध कराई। इस प्रकार हमारे देश की एवं विश्व की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हमने तैयारी करनी होगी। हमारे महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में तथा गृह उद्योगों के माध्यम से मास्क का व्यापक उत्पादन करके हम पूरे विश्व में निर्यात कर सकते है। गुणवत्ता युक्त स्वदेशी सैनिटाइजर, वेन्टीलेटर आदि बनाने के केन्द्र हमारे र्साइंस, तकनीकी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों के विज्ञान विभाग में नहीं हो सकते? स्वदेशी एवं स्वावलम्बन मात्र स्वदेशी वस्तुओं तक सीमित नहीं हैं, स्वदेशी का भाव एवं स्वाभिमान जगाने हेतु इसकी आवश्यकता निश्चित है। परन्तु यहां कुछ उदाहरण दिए, इस प्रकार से अनेक पहलुओं पर कार्य करने पर विचार करना होगा।
चीनी कोरोना विषाणु के इस संकट के समय में हमारे देश के नेतृत्व एवं समाज के अधिकतर वर्ग ने समझदारी का परिचय दिया है इससे भारत का स्थान वैश्विक स्तर पर काफ़ी मजबूत हुआ है। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक समुदाय की भारत से अपेक्षाएं भी बढ़ना स्वाभाविक है।
हमें अपनी सामाजिक और राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा वैश्विक अपेक्षाओं की पूर्ति करने में देश को सक्षम बनाना है तो उसका माध्यम शिक्षा ही हो सकता है। इस दृष्टि से हमारी शिक्षा व्यवस्था को सक्षम बनाना होगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए शिक्षा जगत के नेतृत्व करने वाले निजी शैक्षिक संस्थानों के प्रमुख शिक्षाविद्, शिक्षक आदि ने कटिबद्ध एवं प्रतिबद्ध होकर संयुक्त प्रयास करने से इस महामारी के कारण शिक्षा पर आए संकट को अवसर में बदलने में हम सक्षम हो सकते हैं, साथ ही सरकार एवं समाज के स्तर पर शिक्षा को उच्च प्राथमिकता पर लाना होगा। इसके परिणाम स्वरूप हमारी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से भारत पुनः समर्थ, शक्तिशाली एवं स्वावलम्बी राष्ट्र बनेगा। जिससे मानव एवं विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा।
(लेखक शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव हैं एवं ये उनके निजी विचार हैं)